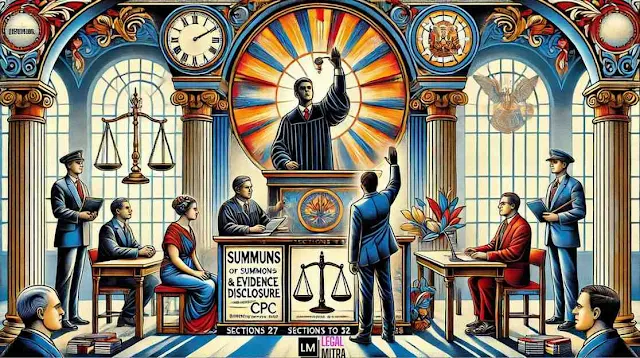सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का भाग 1 साधारणतः वादों के विषय में,रेखांकित करता है तथा इस भाग में धारा 27 से 32 तक को सम्मिलित किया गया है तथा धारा 27 से 32 तक में"समन और प्रकटीकरण (Summons and Discovery) " को रखा गया है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) का भाग 1
वादों की संस्थापन और समन की प्रक्रिया का विवरण देता है। धारा 27
से 32 के तहत वादी और प्रतिवादी को समन जारी
करने, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और सबूतों के
प्रकटीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इन धाराओं का
उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध हो।
“सिविल प्रक्रिया
संहिता, 1908 (CPC) की धारा 27 से 32 के तहत समन और प्रकटीकरण की प्रक्रिया को सरल
और स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इससे वादी, प्रतिवादी और
गवाहों को न्यायिक प्रक्रिया की समझ विकसित करने में सहायता मिलगी”
धारा 27:
समन का जारी किया जाना (Institution of Summons)
अर्थ:
धारा 27 के अनुसार, वाद
की संस्थापन के बाद प्रतिवादी को समन (Summons) जारी किया
जाता है, जिसमें उसे वादपत्र (Plaint) के
साथ उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए निर्देशित किया जाता है।
प्रक्रिया:
1. वादपत्र
दायर करने के बाद न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन जारी किया जाता है।
2. समन
में प्रतिवादी को निर्दिष्ट तिथि पर न्यायालय में उपस्थिति के निर्देश दिए जाते
हैं।
3. समन
में वाद की प्रतिलिपि और उत्तर दायर करने की अंतिम तिथि का उल्लेख किया जाता है।
महत्व:
• यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिवादी को उचित अवसर मिले।
• समन का उद्देश्य पक्षकारों को वाद की जानकारी देना और सुनवाई में
भाग लेने के लिए आमंत्रित करना है।
न्यायिक निर्णय
डॉ. (श्रीमती) नीलम
सिन्हा बनाम उज्जवल कुमार सिन्हा, AIR 2002 Pat 52
प्रासंगिक धारा:
धारा 27
(समन का जारी किया जाना)
निर्णय का सार:
- इस मामले में न्यायालय ने यह
स्पष्ट किया कि समन की सेवा उचित रूप से होनी चाहिए और समन के माध्यम से
प्रतिवादी को वाद की जानकारी देना न्यायिक प्रक्रिया का एक अनिवार्य चरण है।
- समन की उचित सेवा नहीं होने पर
प्रतिवादी के खिलाफ एकतरफा आदेश (Ex-parte
Decree) पारित नहीं किया जा
सकता है।
अर्थ:
धारा 28 के अनुसार, यदि
प्रतिवादी न्यायालय की स्थानीय सीमाओं से बाहर रहता है, तो
समन को न्यायालय की अनुमति से अन्य क्षेत्राधिकार में भी सेवा किया जा सकता है।
प्रावधान:
1. न्यायालय
समन को उस क्षेत्राधिकार के न्यायालय को भेज सकता है,
जहाँ प्रतिवादी निवास करता है।
2. समन
की सेवा के लिए न्यायालय उचित माध्यम (रजिस्ट्री/कूरियर) का उपयोग कर सकता है।
महत्व:
• न्यायालय की स्थानीय सीमाओं से बाहर रहने वाले प्रतिवादी को भी
सुनवाई का समान अवसर मिलता है।
• प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान आवश्यक है।
न्यायिक निर्णय
के. नारायणन बनाम
लक्ष्मी, AIR 1996 Ker 216
प्रासंगिक धारा:
धारा 28
(समन की सेवा का क्षेत्राधिकार)
निर्णय का सार:
- इस मामले में केरल उच्च न्यायालय
ने कहा कि यदि प्रतिवादी न्यायालय की स्थानीय सीमाओं से बाहर रहता है,
तो समन को अन्य क्षेत्राधिकार में भेजना न्यायालय का
विशेषाधिकार है।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि
यदि समन को उचित माध्यम से भेजा जाता है, तो
इसे वैध सेवा माना जाएगा।
धारा 29:
विदेशी क्षेत्राधिकार में समन की सेवा (Service of Foreign
Summons)
अर्थ:
धारा 29 विदेशी क्षेत्राधिकार में समन की सेवा
के लिए प्रावधान करती है। यदि प्रतिवादी भारत से बाहर है, तो
समन की सेवा विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के माध्यम से की जाती है।
प्रावधान:
1. विदेश
में स्थित प्रतिवादी को समन की सेवा के लिए राजनयिक माध्यम अपनाए जाते हैं।
2. न्यायालय
समन को संबंधित देश के राजनयिक अधिकारी या दूतावास के माध्यम से भेजता है।
महत्व:
• सीमा पार विवादों में न्यायिक प्रक्रिया को सक्षम बनाना।
• विदेश में स्थित प्रतिवादी को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करना।
न्यायिक निर्णय
मर्चेंट्स ऑफ
इंडिया बनाम विदेशी व्यापार मंत्रालय, AIR 1983 SC 937
प्रासंगिक धारा:
धारा 29
(विदेशी क्षेत्राधिकार में समन की सेवा)
निर्णय का सार:
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में
कहा कि विदेशी क्षेत्राधिकार में समन की सेवा के लिए राजनयिक माध्यमों का
उपयोग किया जाना चाहिए।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत
सरकार के माध्यम से समन की सेवा करना अंतरराष्ट्रीय नियमों और न्यायिक
प्रक्रिया का पालन करने के लिए आवश्यक है।
अर्थ:
धारा 30 न्यायालय को वाद की सुनवाई के दौरान
समन जारी करने, गवाहों को बुलाने और साक्ष्यों की मांग करने
का अधिकार देती है।
न्यायालय के
अधिकार:
1. गवाहों
को उपस्थित होने का आदेश देना।
2. दस्तावेजों
और साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देना।
3. प्रत्येक
पक्ष को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का उचित अवसर देना।
महत्व:
• सुनवाई में निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
• साक्ष्यों की समुचित जांच और प्रस्तुति के माध्यम से न्याय
प्राप्त करना।
न्यायिक निर्णय
के. एन.
वेंकटाचलैया बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
AIR 1990 SC 2056
प्रासंगिक धारा:
धारा 30
(समन और गवाहों को बुलाने की शक्ति)
निर्णय का सार:
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि धारा 30 के तहत न्यायालय को
गवाहों को समन करने और दस्तावेजों की मांग करने का पूर्ण अधिकार है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि कोई
पक्षकार या गवाह समन का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
धारा 31:
गवाहों को बुलाने का समन (Summons to Witnesses)
अर्थ:
धारा 31 के तहत न्यायालय को यह अधिकार है कि
वह वादी और प्रतिवादी दोनों के अनुरोध पर गवाहों को समन जारी कर सके।
प्रक्रिया:
1. गवाहों
को समन भेजा जाता है, जिसमें सुनवाई की तिथि और
स्थान का उल्लेख किया जाता है।
2. गवाहों
को साक्ष्य प्रस्तुत करने और न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
महत्व:
• गवाहों की उपस्थिति सुनवाई को निष्पक्ष बनाती है।
• प्रमाणों की विश्वसनीयता को परखने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है।
न्यायिक निर्णय
मानसिंह बनाम
हनुमान प्रसाद, AIR 1958 SC 912
प्रासंगिक धारा:
धारा 31
(गवाहों को बुलाने का समन)
निर्णय का सार:
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में
स्पष्ट किया कि गवाहों को समन जारी करना न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया का एक
अभिन्न हिस्सा है।
- यदि गवाह समन के बावजूद उपस्थित
नहीं होता है, तो न्यायालय को उचित
कदम उठाने का अधिकार है।
धारा 32:
गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करना (Penalty for Default of
Witness Attendance)
अर्थ:
धारा 32 के अनुसार, यदि
गवाह न्यायालय द्वारा जारी समन के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है।
न्यायालय के
अधिकार:
1. गवाह
के विरुद्ध गिरफ्तारी का आदेश देना।
2. गवाह
पर जुर्माना लगाना।
3. अनुपस्थिति
की स्थिति में उचित दंड लगाना।
महत्व:
• न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना।
• गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित कर सुनवाई को प्रभावी बनाना।
न्यायिक निर्णय
गिरिराज प्रसाद
बनाम राज्य सरकार, AIR 1976 SC 182
प्रासंगिक धारा:
धारा 32
(गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित करना)
निर्णय का सार:
- इस मामले में न्यायालय ने कहा कि
यदि गवाह समन के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय को धारा 32 के तहत गिरफ्तारी का
आदेश देने या दंड लगाने का अधिकार है।
- यह निर्णय न्यायिक अनुशासन और
निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने में सहायक रहा।
धारा 27
से 32 तक सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
(CPC) में समन और प्रकटीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल
हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता
सुनिश्चित करते हैं। समन जारी करने की प्रक्रिया, गवाहों को
बुलाने और साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के नियम न्यायालय को विवाद का उचित
मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं।
समन की सेवा:
समन
की समय पर और उचित सेवा से प्रतिवादी और गवाहों को न्यायालय में उपस्थित होने का
पर्याप्त अवसर मिलता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया
बाधित नहीं होती।
गवाहों की
उपस्थिति:
गवाहों
की उपस्थिति और साक्ष्यों की प्रस्तुति न्यायालय को विवाद के सभी पहलुओं का
मूल्यांकन करने और न्यायिक निष्कर्ष तक पहुँचने में सहायक होती है।
दंडात्मक प्रावधान:
यदि
गवाह समन की अवहेलना करता है, तो धारा 32 के तहत न्यायालय को दंडात्मक कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है, जिससे न्यायिक अनुशासन और न्याय प्रक्रिया की गरिमा बनी रहती है।
अंततः, इन धाराओं का उद्देश्य न्यायालय को वाद की सुनवाई में आवश्यक औपचारिकताओं
को पूर्ण करने और विवाद के सही समाधान तक पहुँचने में सक्षम बनाना है। समन और
प्रकटीकरण की यह प्रक्रिया सुनवाई की पारदर्शिता, न्यायिक
अनुशासन और निष्पक्ष न्याय को सुनिश्चित करती है, जिससे वादी
और प्रतिवादी दोनों को समान अवसर प्राप्त होते हैं।
FAQs: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) – भाग 1: समन और प्रकटीकरण (Summons and Discovery)
1. समन (Summons)
क्या होता है और इसे कब जारी किया जाता है?
उत्तर:
समन एक कानूनी दस्तावेज है जो न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को वाद की सूचना देने और
न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है। इसे वाद की
संस्थापन (Institution of Suit) के तुरंत बाद जारी
किया जाता है।
2. धारा 27
के तहत समन की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:
- वाद दायर होने के बाद न्यायालय
समन जारी करता है।
- समन में प्रतिवादी को वादपत्र की
प्रतिलिपि और उत्तर देने की अंतिम तिथि के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का
निर्देश दिया जाता है।
3. धारा 28
किस स्थिति में लागू होती है?
उत्तर:
धारा 28
तब लागू होती है जब प्रतिवादी न्यायालय की स्थानीय सीमा (Jurisdiction)
से बाहर निवास करता है। ऐसे मामलों में, समन
को अन्य क्षेत्राधिकार के न्यायालय को सेवा के लिए भेजा जाता है।
4. धारा 29
में विदेशी क्षेत्राधिकार में समन की सेवा कैसे की जाती है?
उत्तर:
- विदेश में स्थित प्रतिवादी को समन
की सेवा भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के माध्यम से की जाती है।
- यह सेवा राजनयिक माध्यमों,
दूतावास या उच्चायोग के माध्यम से की जाती है।
5. धारा 30
के अंतर्गत न्यायालय के समन और साक्ष्य प्रस्तुत करने से संबंधित
क्या अधिकार हैं?
उत्तर:
- न्यायालय गवाहों को समन जारी कर
सकता है।
- साक्ष्यों और दस्तावेजों की
प्रस्तुति का आदेश दे सकता है।
- प्रत्येक पक्ष को उचित अवसर
प्रदान कर सकता है ताकि निष्पक्ष सुनवाई हो सके।
6. गवाहों
को समन जारी करने से संबंधित धारा 31 का उद्देश्य क्या है?
उत्तर:
धारा 31 के तहत न्यायालय को गवाहों को समन
जारी करने का अधिकार है, जिससे गवाहों को सुनवाई में उपस्थित
होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।
7. यदि गवाह
समन का पालन नहीं करता तो न्यायालय धारा 32 के तहत क्या
कार्रवाई कर सकता है?
उत्तर:
- न्यायालय गवाह के विरुद्ध
गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है।
- गवाह पर जुर्माना लगाया जा सकता
है।
- अनुपस्थिति की स्थिति में उचित
दंड लगाया जा सकता है।
8. समन की
सेवा किस माध्यम से की जा सकती है?
उत्तर:
समन की सेवा डाक, कूरियर, राजपत्र या व्यक्तिगत सेवा के माध्यम से की जा सकती है। यदि प्रतिवादी
विदेशी क्षेत्राधिकार में है, तो सेवा राजनयिक माध्यमों से
की जाती है।
9. क्या
प्रतिवादी समन की अवहेलना कर सकता है?
उत्तर:
नहीं,
समन की अवहेलना करने पर न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा
निर्णय (Ex-Parte Decree) पारित कर सकता है, जो प्रतिवादी के लिए हानिकारक हो सकता है।
10. धारा 27
से 32 के तहत समन और प्रकटीकरण का उद्देश्य
क्या है?
उत्तर:
- न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता
और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।
- वादी और प्रतिवादी को विवाद की
जानकारी देना।
- गवाहों को बुलाना और साक्ष्यों का
उचित प्रकटीकरण करना।
11. विदेश
में समन की सेवा की अवधि कितनी होती है?
उत्तर:
विदेश में समन की सेवा की अवधि संबंधित देश और राजनयिक माध्यमों की प्रक्रिया पर
निर्भर करती है। औसतन यह प्रक्रिया 30 से 90
दिन तक का समय ले सकती है।
12. समन और
प्रकटीकरण में देरी होने पर न्यायालय क्या कर सकता है?
उत्तर:
- न्यायालय समन की दोबारा सेवा का आदेश
दे सकता है।
- आवश्यक होने पर,
एकतरफा आदेश या डिक्री पारित कर सकता है।
13. क्या
समन की सेवा ई-मेल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जा सकती है?
उत्तर:
हां,
संशोधित नियमों के तहत समन की सेवा ई-मेल, व्हाट्सएप
और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी की जा सकती है, बशर्ते
कि अदालत की अनुमति प्राप्त हो।
14. क्या
समन की सेवा में त्रुटि होने पर मामला रद्द हो सकता है?
उत्तर:
नहीं,
लेकिन यदि समन की सेवा में त्रुटि होती है तो प्रतिवादी इसे चुनौती
दे सकता है और न्यायालय उचित आदेश पारित कर सकता है।
15. गवाहों
की अनुपस्थिति की स्थिति में क्या दंड लगाया जा सकता है?
उत्तर:
- न्यायालय गवाह की अनुपस्थिति पर
जुर्माना लगा सकता है।
- गवाह की गिरफ्तारी का आदेश भी
दिया जा सकता है।